From Law to Life: SC Weaves Compassion into POCSO Jurisprudence in Adolescent Privacy Case
- M.R Mishra

- May 26, 2025
- 6 min read
(हिंदी अनुवाद नीचे है)
In a decision that harmonizes statutory rigidity with constitutional compassion, the Supreme Court in In Re: Right to Privacy of Adolescents (2025) rewrote the script on how the law should respond to adolescent relationships. With piercing clarity and extraordinary empathy, the Court refused to send a convicted man to prison for a statutory offence under the POCSO Act, where the prosecutrix then a minor is now his partner, co-parent, and committed spouse. Exercising its extraordinary powers under Article 142, the Court ensured that law did not become a bludgeon against the very person it sought to protect.
What's The Matter?
The genesis of the case lay in a deeply familiar paradox: a 14-year-old girl entered into a relationship with a 25-year-old man. She eloped, bore a child, and despite her family’s abandonment, continued to live with the man, ultimately forming what she considers a stable family unit.
Statutorily, it was a clear violation penetrative sexual assault under Section 6 of the POCSO Act and Section 376(2)(n) and (3) IPC. The Trial Court convicted the man.
Section 6 of the POCSO Act punishes aggravated penetrative sexual assault against children with a minimum of 20 years to life imprisonment, and potentially the death penalty in severe cases. Section 376(2)(n) IPC addresses repeated rape on the same woman, mandating 10 years to life imprisonment. Section 376(3) IPC covers rape of a minor under 16, prescribing 20 years to life imprisonment.
The POCSO Act is a special law for child protection, while the IPC is a general law for various offenses, including rape.

What's Happened in Court?
The High Court, in a sweeping use of its Article 226 and Section 482 CrPC powers, set aside the conviction on grounds of cohabitation and mutual desire to raise the child.
That reasoning prompted a Suo Motu PIL from the Supreme Court a rare intervention in an individual criminal appeal. What followed was judicial process at its most human.
The Court appointed a committee of experts from TISS and other public institutions, whose final report read more like a social audit than a legal brief. It narrated the tragic sequence of systemic abandonment: the girl had no informed choice, no parental support, and no state protection.
Ostracized by her village, surveilled by her family, and tossed between institutions, she chose to remain with the only one who offered continuity the accused. She later spent over ₹2 lakh in court fees, tout payments, and travel to save him from jail. Her trauma, the committee said, was not from the relationship, but from the legal fallout and institutional apathy.
With sensitivity rarely seen in statutory sentencing, the Court acknowledged that enforcing the minimum 20-year sentence would hurt the very person the law aimed to protect. It did not deny the commission of the offence. It did not dilute the statutory minimum. Instead, invoking Article 142, it exercised constitutional equity to hold that no further sentence would be imposed, though the conviction stood. In doing so, it upheld the law but bent it to serve justice.
The decision is not a precedent, the Court was quick to say. It is, rather, an urgent corrective to a particular failure—of society, state, and legal institutions. But its implications echo widely. It casts a long shadow on the criminalization of consensual adolescent relationships and presses for a nuanced application of the POCSO Act in cases where prosecutrixes no longer see themselves as victims.
Beyond sentencing, the Court mandated a welfare model. The State of West Bengal was directed to provide shelter, education up to graduation, vocational training, and financial support for the girl and her child. The Court also issued broader directions: to the Union of India, to create expert bodies, integrate adolescent-focused education reforms, and establish data-driven accountability mechanisms.
The judgment transforms the court from a passive adjudicator into an active architect of rehabilitation and adolescent protection.When the law criminalizes care, the court must humanize it. And in this rare instance, the Supreme Court has done just that.
कानूनी कठोरता और संवैधानिक संवेदनशीलता के सामंजस्य में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इन री: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स (2025) के मामले में एक ऐसा निर्णय दिया जो कानून की कठोरता और संविधान की मानवीय भावना के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कोर्ट ने असाधारण स्पष्टता और संवेदनशीलता दिखाते हुए POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को जेल भेजने से इनकार कर दिया, जहाँ पीड़िता (जो उस समय नाबालिग थी) अब उसकी जीवनसाथी, सह-अभिभावक और प्रतिबद्ध पत्नी है।
अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि कानून उसी व्यक्ति के खिलाफ एक दंडात्मक हथियार न बन जाए, जिसकी रक्षा के लिए वह बना था।
मामला क्या था?
यह मामला एक सामान्य लेकिन विडंबनापूर्ण स्थिति से उपजा: एक 14 वर्षीय लड़की ने 25 वर्षीय व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाया। वह उसके साथ भाग गई, उससे एक बच्चा हुआ, और परिवार द्वारा त्याग दिए जाने के बावजूद, वह उसी के साथ रहती रही और आज उनका एक स्थिर परिवार है।
कानूनी तौर पर, यह POCSO एक्ट की धारा 6 (बच्चों के साथ गंभीर यौन हिंसा) और IPC की धारा 376(2)(n) व 376(3) (नाबालिग के साथ बलात्कार) का स्पष्ट उल्लंघन था। ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया।
POCSO की धारा 6 बच्चों के साथ गंभीर यौन हिंसा के लिए कम से कम 20 साल से आजीवन कारावास (और गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक) की सजा निर्धारित करती है।
IPC की धारा 376(2)(n) एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार के लिए 10 साल से आजीवन कारावास की सजा देती है।
IPC की धारा 376(3) 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए 20 साल से आजीवन कारावास का प्रावधान करती है।
(POCSO एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून है, जबकि IPC बलात्कार सहित अन्य अपराधों के लिए एक सामान्य कानून है।)
कोर्ट में क्या हुआ?
हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 226 और CrPC की धारा 482 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दोनों के सहवास और बच्चे को पालने की इच्छा के आधार पर सजा को रद्द कर दिया।
इसी तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu PIL) लिया एक व्यक्तिगत आपराधिक मामले में यह एक दुर्लभ हस्तक्षेप था। इसके बाद जो हुआ, वह न्यायिक प्रक्रिया का सबसे मानवीय पक्ष था।
कोर्ट ने TISS और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट कानूनी दस्तावेज़ से ज्यादा एक सामाजिक अध्ययन जैसी थी। इसमें उस लड़की की दुर्दशा का वर्णन था: उसके पास न तो सही विकल्प थे, न ही परिवार का सहारा, और न ही राज्य की सुरक्षा।
गाँव द्वारा बहिष्कृत, परिवार द्वारा निगरानी किए जाने और संस्थानों के बीच झुलसने के बाद, उसने उसी व्यक्ति के साथ रहना चुना जिसने उसे स्थिरता दी आरोपी। बाद में, उसने 2 लाख रुपये से अधिक कोर्ट फीस, दलालों और यात्रा में खर्च किए ताकि उसे जेल न जाना पड़े।
समिति ने कहा कि उसका आघात रिश्ते से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया और संस्थागत उपेक्षा से हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए माना कि 20 साल की अनिवार्य सजा लागू करना उसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाएगा जिसकी रक्षा के लिए कानून बना था।
उसने अपराध होने से इनकार नहीं किया, न ही सजा को कम किया। बल्कि, अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक न्याय का प्रयोग करते हुए, कोर्ट ने फैसला दिया कि दोषसिद्धि बनी रहेगी, लेकिन कोई और सजा नहीं दी जाएगी।
इस तरह, उसने कानून को बरकरार रखा, लेकिन न्याय के लिए उसमें लचीलापन दिखाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला एक मिसाल (precedent) नहीं, बल्कि समाज, राज्य और कानूनी संस्थानों की एक विशेष विफलता का एक तात्कालिक सुधार है।
लेकिन इसके निहितार्थ व्यापक हैं यह सहमति से बने किशोर रिश्तों के अपराधीकरण पर सवाल उठाता है और POCSO एक्ट के उन मामलों में संवेदनशील लागू करने की माँग करता है जहाँ पीड़िता अब खुद को शिकार नहीं मानती।
सजा से आगे: कल्याणकारी मॉडल
कोर्ट ने केवल सजा पर फैसला ही नहीं दिया, बल्कि एक कल्याणकारी मॉडल भी तैयार किया। पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया गया कि वह लड़की और उसके बच्चे को आश्रय, स्नातक तक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करे।
साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए:
विशेषज्ञ समितियाँ बनाने,
किशोर-केंद्रित शिक्षा सुधारों को लागू करने, और
डेटा-आधारित जवाबदेही तंत्र स्थापित करने के लिए।
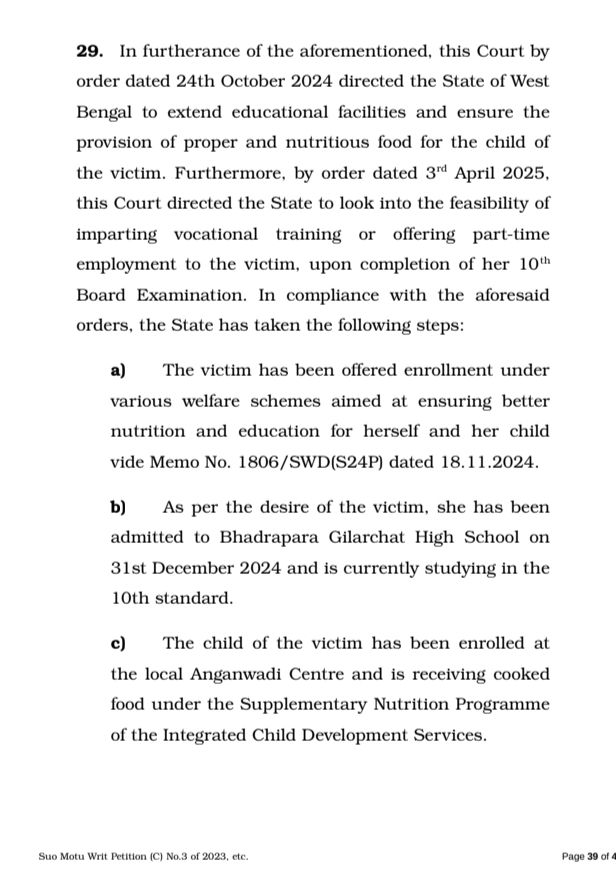
यह निर्णय कोर्ट की भूमिका को एक निष्क्रिय न्यायाधीश से बदलकर एक सक्रिय पुनर्वास-निर्माता बना देता है। जब कानून देखभाल को अपराध बना दे, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उसे मानवीय बनाए। और इस दुर्लभ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक यही किया।




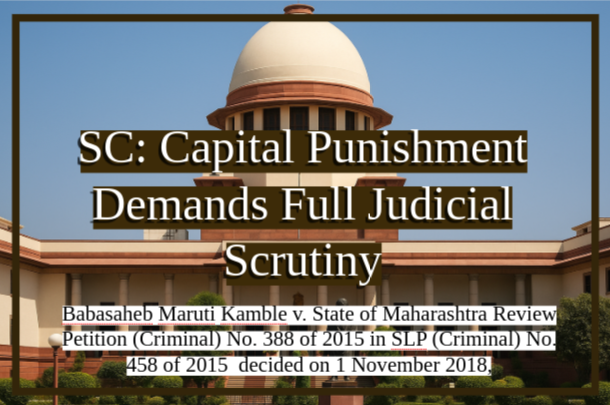


Comments